Radio Veritas Asia Buick St., Fairview Park, Queszon City, Metro Manila. 1106 Philippines | + 632 9390011-15 | +6329390011-15
संत पापा ने कहा स्तोत्र, प्रार्थना की एक पाठशाला!
बुधवरीय आमदर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्राँसिस ने स्तोत्र ग्रंथ की प्रार्थना पर चिंतन किया। उन्होंने कहा कि स्तोत्र हमें ईश्वर की नजरों से सच्चाई पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है।
संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पौल षष्ठम के सभागार में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को सबोधित करते हुए कहा, प्रिय भाई एवं बहनो सुप्रभात।
आज की धर्मशिक्षा माला में हम स्तोत्र की प्रार्थना का समापन करेंगे। स्तोत्र में हम एक नकारात्मक व्यक्तित्व को पाते हैं जिसे हम “दुष्ट” व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं जो अपने जीवन को इस भांति जीता है मानो ईश्वर हैं ही नहीं। हम उस व्यक्ति के किसी पारलौकिक सन्दर्भ को नहीं पाते जिसमें असीमित अहंकार है, जिसे अपने कार्यों और विचारों के न्याय का कोई भय नहीं है।
यही कारण है कि स्तोत्र लेखक प्रार्थना को जीवन की एक मूलभूत सच्चाई स्वरुप व्यक्त करते हैं। उस दिव्य और आलौकिक व्यक्तित्व को आध्यात्मिक गुरू “ईश्वर का पवित्र भय” निरूपित करते हैं जो हमें पूर्ण मानव बनाता है क्योंकि यह एक सीमांत की भांति हमें अपने जीवन को अंधाधुंध, एक हिंसक मानव की तरह जीने से रोकता है। प्रार्थना में हम मानव जाति की मुक्ति को पाते हैं।
प्रशंसा की खोज, झूठी प्रार्थना
संत पापा ने कहा कि वहीं एक झूठी प्रार्थना भी है, एक प्रार्थना जो दूसरों से प्रशंसा की खोज करती है। कुछ लोग अपने को ख्रीस्तीय दिखाने या उन्होंने क्या नया खरीदा है उसकी नुमाईश हेतु गिरजा जाते हैं जो एक झूठी प्रार्थना है। येसु इस तरह की प्रार्थना का घोर प्रतिकार करते हैं (मत्ती. 6.5-6, लूका. 9.14)। सच्ची प्रार्थना अपनी निष्ठा में हृदय की गहराई में उतरता जहाँ हम सच्चाई को ईश्वर की निगाहों से देखते हैं।
प्रार्थना जीवन की गहराई
जब कोई प्रार्थना करता है तो वह अपने जीवन की सभी चीजों को “गहराई” से देखता है। इसमें एक उत्सुकता होती है जो छोटी चीज से शुरू होते हुए अपनी गहराई में जाती है मानो ईश्वर ने उस छोटी चीज को अपने हाथों में उठा कर उसे बदल दिया हो। हमारे लिए सबसे खराब, आदतन रूप में तोते की तरह प्रार्थना करना है, जो नहीं होना चाहिए। हमें हृदय से प्रार्थना करने की जरुरत है क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का क्रेन्द-विन्दु है। संत पापा ने कहा कि यदि हमारी प्रार्थना ऐसी होती, तो हमारे भाई-बहन और हमारे शत्रु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राचीन मठवासी ख्रीस्तियों की एक कहावत है, “धन्य है वह मठवासी जो ईश्वर के बाद सभी मनुष्यों को ईश्वर के प्रतिरुप में देखा है” (एवरग्रीयुस पोंटिकस, प्रार्थना,122)। जो ईश्वर की आराधना करते हैं वे उनकी संतानों से प्रेम करते हैं। वे जो ईश्वर का सम्मान करते मानव जाति का सम्मान करते हैं।
प्रार्थना, उत्तरदायित्व का एहसास
अतः प्रार्थना कोई चिंता निवारक साधन नहीं है और न ही ऐसी प्रार्थना सही अर्थ में ख्रीस्तीय प्रार्थना है। प्रार्थना, अपितु हममें से हर एक को उत्तरदायी व्यक्ति बनाती है। इसे हम “हे पिता हमारे” की प्रार्थना में पाते हैं जिसे येसु ने अपने शिष्यों को सिखलाया।
भजनमाला एक विद्यालय की भांति है जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देती है। स्तोत्र सदैव परिशुद्ध और कोमल भाषा का उपयोग नहीं करते, वे हमारे लिए जीवन की निशानियों को बहुधा व्यक्त करते हैं। इसके बावजूद, उन सारी व्यक्तिगत और हृदय की आंतरिक गहराई से निकली प्रार्थनाओं का उपयोग पहले येरुसलेम के मंदिरों और उसके बाद यहूदियों के प्रार्थनागृहों में होता था। काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा इसके बारे में कहती है, “स्तोत्र की प्रार्थना का स्वरुप मंदिर और मानव हृदय दोनों में तैयार होते हैं” (2588)। इस भांति व्यक्तिगत प्रार्थना इस्राएलियों के जीवन से उत्पन्न और पोषित होते तथा कलीसिया की प्रार्थना का रुप बनते हैं।
स्तोत्र में दिल की भावनाएं
स्तोत्र में एकवचन, व्यक्ति के व्यक्तिगत अंतरंग विचारों और समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है, जो एक सामूहिक विरासत है जिसका उपयोग हर कोई और हर किसी के लिए प्रार्थना हेतु किया जाता है। ख्रीस्तीय प्रार्थना में ऐसी “सांस” और आध्यात्मिक “तनाव” का मिश्रण है जो मंदिर और विश्व को एक साथ पकड़ कर रख सकती है। प्रार्थना गिरजाघर के गुबंदों से शुरू होते हुए शहरों की गलियों में इति हो सकती है। और इसके विपरीत यह दिनचर्या कार्यों की चिंताओं में पुलकित होते हुए धर्मविधि की पूरिपूर्ण में पाई जाती है। कलीसिया के द्वार अवरोधक नहीं लेकिन भेद्य “झिल्लियाँ” हैं जहाँ हरएक की गुहार का स्वागत किया जाता है।
स्तोत्र प्रार्थना में हम दुनिया की उपस्थिति को सदैव पाते हैं। उदाहरण स्वरुप स्तोत्रों में हम, अति कमजोर लोगों की मुक्ति हेतु दिव्य याचना की प्रतिज्ञा पाते हैं। “क्योंकि गरीब सताये जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं, प्रभु कहता है, मैं अब उठूँगा, मैं उनका उद्धार करूँगा” (12.5)। स्तोत्र मनुष्य को दुनियादारी से सचेत करते हैं, “मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता वह पशुओं की भांति है जिसका विनाश होता है” (49.20)। स्तोत्रों में हम ईश्वरीय क्षीतिज को खुलता सुनते हैं, “प्रभु राष्ट्रों की योजना व्यर्थ करता है और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। किन्तु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी बने रहते हैं” (33.10-11)
प्रार्थना का सार, पड़ोसी प्रेम
संत पापा ने कहा कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जहाँ ईश्वर हैं, वहाँ मानव का होना जरुरी है। पवित्र धर्मग्रंथ अपने में सुस्पष्ट है, “हम प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पहले प्रेम किया है। यदि कोई कहता है, मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ, और वह अपने भाई से घृणा करता है तो वह झूठा है, क्योंकि यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है प्रेम नहीं करता, तो ईश्वर को जिसे वह नहीं देखता है कैसे प्रेम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप दिन में कई बार रोजरी करते हैं, लेकिन दूसरों की निंदा शिकायत करते, दूसरों से घृणा के भाव रखते, तो यह सत्य नहीं वरन दिखावा है। यह आज्ञा हमें ईश्वर की ओर से मिली है वह जो ईश्वर को प्रेम करता है वह अपने भाई को भी प्रेम करे”(1 यो.4.19-21)। धर्मग्रंथ हमें एक व्यक्ति के हाल से रुबरू कराता है जो निष्ठा में ईश्वर की खोज करता लेकिन उसका साक्षात्कार ईश्वर से नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए यह भी सुस्पष्ट किया जाता है कि गरीबों की आंसुओं को हम कभी अनदेखा न करें, क्योंकि हमारा साक्षात्कार ईश्वर से नहीं हुआ है। ईश्वर उस “अविश्वास” को बढ़वा नहीं देते जो मानव में दिव्य उपस्थिति को नकारता हो। मेरा ईश्वर में विश्वास है लेकिन मैं लोगों से दूरी बनाये रखता, उनसे घृणा करता हूँ तो यह स्थापित अविश्वास है। मानव को ईश्वर के प्रतिरुप में नहीं पहचानना एक अपवित्रीकरण, एक घृणा है, यह अपने में एक बड़ी बुराई है।
संत पापा ने इस चेतावनी के साथ अपनी धर्मशिक्षा का समापन किया, स्तोत्र के माध्यम प्रार्थना करना हमें “दुष्टों” की तरह परीक्षा में पड़ने से बचाये अर्थात हम अपने जीवन को इस तरह न जीयें मानो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं और न ही गरीबों का अस्तित्व है।
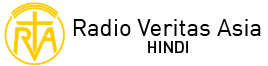



Add new comment